International Journal of Sanskrit Research
2017, Vol. 3, Issue 6, Part A
साहितà¥à¤¯ धरà¥à¤®
डाॅ0 अशोक कà¥à¤®à¤¾à¤° दà¥à¤¬à¥‡
संसà¥à¤•à¥ƒà¤¤à¤à¤¾à¤·à¤¾ के शबà¥à¤¦à¥‹à¤‚ का वैशिषà¥à¤Ÿà¥à¤¯ यह है कि पà¥à¤°à¤¾à¤¯à¤ƒ वà¥à¤¯à¥à¤¤à¥à¤ªà¤¤à¥à¤¤à¥à¤²à¤¿à¤à¥à¤¯ अरà¥à¤¥ में अपनी परिà¤à¤¾à¤·à¤¾ à¤à¥€ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤ करते हैं। यह तथà¥à¤¯ ‘साहितà¥à¤¯â€™ और ‘धरà¥à¤®â€™ इन दोनों शबà¥à¤¦à¥‹à¤‚ में à¤à¥€ अनà¥à¤µà¤°à¥à¤¥à¤• है। साहितà¥à¤¯ हैं सहित का à¤à¤¾à¤µ और सहित है- हित के साथ (हितेन यह सहितमà¥)। इसी पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤° धरà¥à¤® शबà¥à¤¦ धृ धातà¥-से निपनà¥à¤¨ है, जिसका अरà¥à¤¥-धारण करना है-(धरति धियते व धरà¥à¤®à¤ƒ)। सà¥à¤µà¤à¤¾à¤µ, नà¥à¤¯à¤¾à¤¯, आधार आदि इसके अनेक परà¥à¤¯à¤¾à¤¯ है। किसी वसà¥à¤¤à¥ की विधायक आनà¥à¤¤à¤°à¤¿à¤• वृतà¥à¤¤à¤¿ को धरà¥à¤® कहते हैं। पà¥à¤°à¤¤à¥à¤¯à¥‡à¤• पदारà¥à¤¥ का वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¤à¥à¤µ जिस वृतà¥à¤¤à¤¿ पर निरà¥à¤à¤° है, वही उस पदारà¥à¤¥ का धरà¥à¤® है। धरà¥à¤® की कमी से उस पदारà¥à¤¥ का कà¥à¤·à¤¯ होता है और धरà¥à¤® की वृदà¥à¤§à¤¿ होती है। बेले के फूल का धरà¥à¤® सà¥à¤µà¤¾à¤¸ है, उसकी वृदà¥à¤§à¤¿, उसकी कली का विकास है, उसकी कमी फूल का हà¥à¤°à¤¾à¤¸ ह। धरà¥à¤® की परिकलà¥à¤ªà¤¨à¤¾ à¤à¤¾à¤°à¤¤ की अपनी विशेषता है। मानवीय वà¥à¤¯à¤µà¤¹à¤¾à¤° आदि के संदरà¥à¤ में धरà¥à¤® अतà¥à¤¯à¤¨à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤¾à¤ªà¤• अरà¥à¤¥ में à¤à¤¾à¤°à¤¤à¥€à¤¯ मनीषियों दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ पà¥à¤°à¤¯à¥à¤•à¥à¤¤ होता रहा है, जो वैदिक अनà¥à¤·à¥à¤ ान, करà¥à¤¤à¤µà¥à¤¯, धरà¥à¤®, विधि, नियम, पूजापदà¥à¤§à¤¤à¤¿ आदि के परà¥à¤¯à¤¾à¤¯ के रूप में पà¥à¤°à¤¸à¤¿à¤¦à¥à¤§ है। धातà¥à¤µà¤°à¥à¤¥ की दृषà¥à¤Ÿà¤¿ से इसका केनà¥à¤¦à¥à¤°à¥€à¤¯ अरà¥à¤¥ है-जड़ तथा चेतन दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ धारित ततà¥à¤µà¥¤ साहितà¥à¤¯ के साथ सामाजिक उतà¥à¤¤à¤° पद के रूप में धरà¥à¤® का अरà¥à¤¥ पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤à¥à¤¤ लेख में सà¥à¤µ-à¤à¤¾à¤µ मानकर विवेचन किया गया है।
Pages : 36-38 | 1098 Views | 137 Downloads
How to cite this article:
डाॅ0 अशोक कà¥à¤®à¤¾à¤° दà¥à¤¬à¥‡. साहितà¥à¤¯ धरà¥à¤®. Int J Sanskrit Res 2017;3(6):36-38.
Related Links
Related Journal Subscription
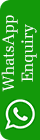

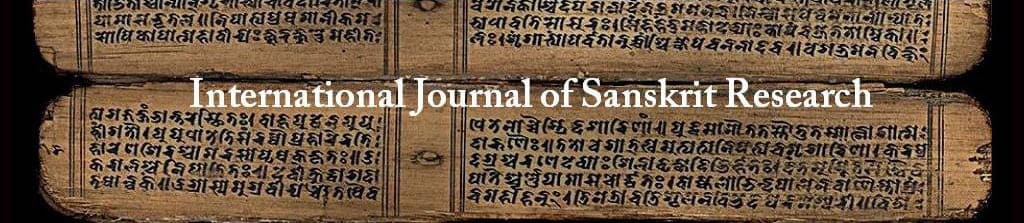



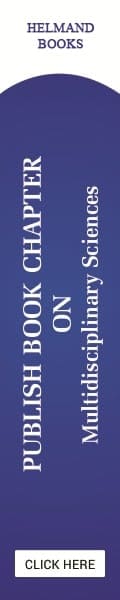
 Research Journals
Research Journals