International Journal of Sanskrit Research
2017, Vol. 3, Issue 3, Part G
सà¥à¤®à¥ƒà¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ में पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤ªà¤¾à¤¦à¤¿à¤¤ विधि वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾ की वरà¥à¤¤à¤®à¤¾à¤¨ काल में पà¥à¤°à¤¾à¤¸à¥œà¥à¤—िकता
Dr. Atiya Danish
वसà¥à¤¤à¥à¤¤à¤ƒ सà¥à¤®à¥ƒà¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ में जिस विधि वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾ का पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤ªà¤¾à¤¦à¤¨ किया गया है वहाठकी संसà¥à¤•à¥ƒà¤¤à¤¿ में धरà¥à¤® की पà¥à¤°à¤§à¤¾à¤¨à¤¤à¤¾ है और वह समाज मूलà¥à¤¯à¥‹à¤‚ पर आधारित है। समाज की संरचना इस आधार इस आधार पर की गई है कि मूलà¥à¤¯à¥‹à¤‚ की सरà¥à¤µà¥‹à¤šà¥à¤šà¤¤à¤¾ बनी रहे और उनमें कोई गिरावट न आये। à¤à¤¾à¤°à¤¤à¥€à¤¯ समाज की आवशà¥à¤¯à¤•à¤¤à¤¾, परिसà¥à¤¥à¤¿à¤¤à¤¿ और परिवेश का धà¥à¤¯à¤¾à¤¨ रखते हà¥à¤ नीति और धरà¥à¤® पर आधारित वरà¥à¤£à¤¾à¤¶à¥à¤°à¤® वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾ बनाई गई और उस वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾ में मानव का जीवन हर पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤° से सà¥à¤°à¤•à¥à¤·à¤¿à¤¤ और नियनà¥à¤¤à¥à¤°à¤¿à¤¤ हो इसकी वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾ की गई है। धरà¥à¤® जहाठà¤à¤• ओर आतà¥à¤®à¤¾ और परमातà¥à¤®à¤¾ के विषय में जानकारी देता है वहीं दूसरी ओर अनà¥à¤¶à¤¾à¤¸à¤¿à¤¤ रहने का सनà¥à¤¦à¥‡à¤¶ à¤à¥€ देता है। मनà¥à¤·à¥à¤¯ और समाज अनà¥à¤¶à¤¾à¤¸à¤¿à¤¤ रहे इसीलिठविधि वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾ की गई। उलà¥à¤²à¥‡à¤–नीय है कि à¤à¤¾à¤°à¤¤ विशà¥à¤µ का वह पà¥à¤°à¤¥à¤® देश है जहाठउस सà¥à¤¦à¥‚र अतीत में à¤à¥€ सà¥à¤®à¥ƒà¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ के रूप में लिखित विधान बनाया गया। उकà¥à¤¤ विधि वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾ की आधर सà¥à¤¥à¤²à¥€ जो सà¥à¤®à¥ƒà¤¤à¤¿à¤¯à¤¾à¤‚ हैं वे à¤à¤• सà¥à¤¦à¥€à¤°à¥à¤˜ कालावाधि तथा विसà¥à¤¤à¥ƒà¤¤ à¤à¥Œà¤—ोलिक परिधि की रचनाà¤à¤‚ हैं। उकà¥à¤¤ सà¥à¤®à¥ƒà¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ में कहीं-कहीं मतवैविधà¥à¤¯ का कारण सà¥à¤®à¥ƒà¤¤à¤¿à¤•à¤¾à¤°à¥‹à¤‚ के सामाजिक दृषà¥à¤Ÿà¤¿à¤•à¥‹à¤£ के पà¥à¤°à¤¤à¤¿ विà¤à¤¿à¤¨à¥à¤¨à¤¤à¤¾ और चिनà¥à¤¤à¤¨ के साथ-साथ उनके समय, परिसà¥à¤¥à¤¿à¤¤à¤¿ और बदलता हà¥à¤† परिवेश à¤à¥€ उसके लिठउतà¥à¤¤à¤°à¤¦à¤¾à¤¯à¥€ है। यही कारण है कि पà¥à¤°à¤¥à¤® सà¥à¤®à¥ƒà¤¤à¤¿à¤•à¤¾à¤° मनॠसे पà¥à¤°à¤¾à¤°à¤®à¥à¤ कर अरà¥à¤µà¤¾à¤šà¥€à¤¨ सà¥à¤®à¥ƒà¤¤à¤¿à¤•à¤¾à¤° की विधि वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾ विषय में मूल à¤à¤¾à¤µà¤¨à¤¾ होने पर à¤à¥€ यंतà¥à¤°-तंतà¥à¤° आवशà¥à¤¯à¤• परिवरà¥à¤¤à¤¨ तथा à¤à¤¿à¤¨à¥à¤¨à¤¤à¤¾ à¤à¥€ दृषà¥à¤Ÿà¤¿à¤—ोचर होती है। वरà¥à¤¤à¤®à¤¾à¤¨ काल में à¤à¥€ विशà¥à¤µ में जहाà¤-जहाठलिखित संविधान हैं वहाठसंविधान में संशोधन की वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾ à¤à¥€ की गई है। यही कारण है कि संविधानों में समय-समय पर संशोधन à¤à¥€ होते रहते हैं। सà¥à¤®à¥ƒà¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ में पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤ªà¤¾à¤¦à¤¿à¤¤ विधि-वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾ और वरà¥à¤¤à¤®à¤¾à¤¨ कालीन संविधान में लगà¤à¤— समानता हैं- समानता इस बात की है कि मौलिक अधिकार, वà¥à¤¯à¤µà¤¹à¤¾à¤°, दणà¥à¤¡, समà¥à¤ªà¤¤à¥à¤¤à¤¿ और जीवन से समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤¿à¤¤ आवशà¥à¤¯à¤• समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¥‹à¤‚ के निरà¥à¤§à¤¾à¤°à¤£ के लिठकानून बनाने की वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾ है। सà¥à¤®à¥ƒà¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ में जिस पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤° राजा को आवशà¥à¤¯à¤•à¤¤à¤¾à¤¨à¥à¤¸à¤¾à¤° (विधि उपलबà¥à¤§ न होने पर) विधि बनाने का अधिकार था, उसी पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤° वरà¥à¤¤à¤®à¤¾à¤¨ काल में देश के नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ को यह देखने का और निशà¥à¤šà¤¿à¤¤ करने का अधिकार दिया गया है कि संसद जो कानून बनाती है, वह संविधान के अनà¥à¤°à¥‚प है या नहीं और यदि नहीं है तो उसे गैरकानूनी घौषित कर देती है। कà¤à¥€-कà¤à¥€ कानून उपलबà¥à¤§ न होने की सà¥à¤¥à¤¿à¤¤à¤¿ में नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤§à¥€à¤¶ सà¥à¤µà¤¯à¤‚ कानून की वà¥à¤¯à¤¾à¤–à¥à¤¯à¤¾ पर नया कानून बना देते हैं शà¥à¤°à¤¨à¤•à¤¹à¤® डंकम सà¥à¤‚ू जिसे कहते हैं। विधि की आवशà¥à¤¯à¤•à¤¤à¤¾ हर समय रही है। पà¥à¤°à¤¾à¤šà¥€à¤¨ काल से लेकर अब तक किसी न किसी रूप में कोई न कोई संसà¥à¤¥à¤¾ या वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ सारà¥à¤µà¤à¥Œà¤® सतà¥à¤¤à¤¾ का अधिकारी रहा। à¤à¤¾à¤°à¤¤ में सदा ही राजा को नियनà¥à¤¤à¥à¤°à¤¿à¤¤ करने और तानाशाह बनने से रोकने के लिठसà¤à¤¾ और समिति कारà¥à¤¯ करती रही है। इसलिठà¤à¤¾à¤°à¤¤ में कà¤à¥€ राजा निरंकà¥à¤¶ नहीं हो सकता यदà¥à¤¯à¤ªà¤¿ उसे इनà¥à¤¦à¥à¤°, यम, कà¥à¤¬à¥‡à¤°, अगà¥à¤¨à¤¿ आदि देवों का अंश अरà¥à¤¥à¤¾à¤¤à¥ दैवी शकà¥à¤¤à¤¿ समà¥à¤ªà¤¨à¥à¤¨ माना गया है। यूरोपीय देशों में राजा दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ में राजा दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ मà¥à¤‚ह से बोला हà¥à¤† शबà¥à¤¦ ही कानून था। उसके ऊपर कोई नियनà¥à¤¤à¥à¤°à¤£ नहीं था इसी कारण यूरोपीय राजनैतिक विजà¥à¤žà¤¾à¤¨ à¤à¤¸à¥‡ निरंकà¥à¤¶ राजाओं के नामों से à¤à¤°à¤¾ पड़ा है। आधà¥à¤¨à¤¿à¤• राजनैतिक विचारकों ने चिनà¥à¤¤à¤¨ करने के पशà¥à¤šà¤¾à¤¤à¥ कानून बनाने का अधिकार जन पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¨à¤¿à¤§à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ को सौंप दिया। फà¥à¤°à¤¾à¤‚स की राजà¥à¤¯ कà¥à¤°à¤¾à¤¨à¥à¤¤à¤¿ के बाद जब राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€à¤¯ राजà¥à¤¯à¥‹à¤‚ का निरà¥à¤®à¤¾à¤£ होना पà¥à¤°à¤°à¤®à¥à¤ हà¥à¤† तो लिखित कानून दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ शासन किया जाने लगा जबकि à¤à¤¾à¤°à¤¤ में यह लिखित कानून मनà¥à¤¸à¥à¤®à¥ƒà¤¤à¤¿ के रूप में दो सहसà¥à¤° वरà¥à¤·à¥‹à¤‚ से à¤à¥€ अधिक पà¥à¤°à¤¾à¤šà¥€à¤¨ है। सà¥à¤ªà¤·à¥à¤Ÿ है कि सà¥à¤®à¥ƒà¤¤à¤¿ साहितà¥à¤¯ में पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤ªà¤¾à¤¦à¤¿à¤¤ विधि-वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾ पूरà¥à¤£à¤¤à¤¯à¤¾ परिवरà¥à¤¤à¤¿à¤¤ काल में à¤à¥€ अनेक अंशों में पà¥à¤°à¤¾à¤¸à¤™à¤¿à¤—क है तो कà¥à¤› कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°à¥‹à¤‚ में मारà¥à¤—दरà¥à¤¶ à¤à¥€à¥¤ उदाहरणतया विधिवेता, विधि निरà¥à¤§à¤¾à¤°à¤• और कहीं-कहीं विधिकरà¥à¤¤à¤¾ राजा केवल वंशपरमà¥à¤ªà¤°à¤¾ के गौरव से ही उकà¥à¤¤ अधिकारों को पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ नहीं करता था, उसके लिठअपेकà¥à¤·à¤¿à¤¤ योगà¥à¤¯à¤¤à¤¾ का होना आवशà¥à¤¯à¤• था, उसे à¤à¤• निरà¥à¤§à¤¾à¤°à¤¿à¤¤ समय सारणी के अनà¥à¤¸à¤¾à¤° निशà¥à¤šà¤¿à¤¤ पदà¥à¤§à¤¤à¤¿ में जीवन-यापन करना होता था। उसका जीवन à¤à¥‹à¤— का नहीं था, वासà¥à¤¤à¤µà¤¿à¤• अरà¥à¤¥à¥‹à¤‚ में वह पà¥à¤°à¤œà¤¾ के लिठथा, पà¥à¤°à¤œà¤¾ का था, सिंहासन चाहे वंश परमà¥à¤ªà¤°à¤¾ से कà¥à¤¯à¥‹à¤‚ न मिला हो। वरà¥à¤¤à¤®à¤¾à¤¨ काल में विधिवेतà¥à¤¤à¤¾, विधिकरà¥à¤¤à¤¾ अधिकारियों के सनà¥à¤¦à¤°à¥à¤ में à¤à¥€ à¤à¤¸à¤¾ ही अनà¥à¤¶à¤¾à¤¸à¤¨ तथा नियमावली सरà¥à¤µà¤¥à¤¾ सà¥à¤µà¤¾à¤—तयोगà¥à¤¯ है।
Pages : 393-396 | 1158 Views | 189 Downloads

How to cite this article:
Dr. Atiya Danish. सà¥à¤®à¥ƒà¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ में पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤ªà¤¾à¤¦à¤¿à¤¤ विधि वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾ की वरà¥à¤¤à¤®à¤¾à¤¨ काल में पà¥à¤°à¤¾à¤¸à¥œà¥à¤—िकता. Int J Sanskrit Res 2017;3(3):393-396.
Related Links
Related Journal Subscription
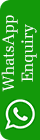

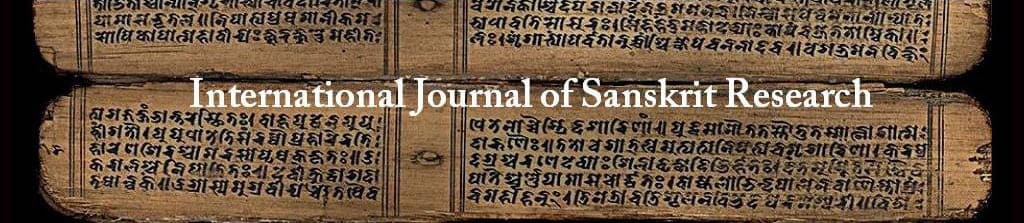



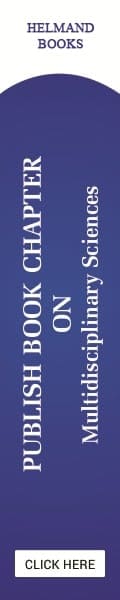
 Research Journals
Research Journals